संन्यास आश्रम की व्यवस्था क्यों- sannyaas aashram kee vyavastha kyon- भारतीय संस्कृति में संन्यास आश्रम का बहुत अधिक महत्त्व है। जीवन के चा...
संन्यास आश्रम की व्यवस्था क्यों-sannyaas aashram kee vyavastha kyon-
भारतीय संस्कृति में संन्यास आश्रम का बहुत अधिक महत्त्व है। जीवन के चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से मोक्षप्राप्ति का साधन संन्यास आश्रम ही है।
● मोक्ष का अर्थ है-समस्त कामनाओं का समाप्त हो जाना और कामनाओं से मुक्त होने के लिए जो साधन या अभ्यास किया जाता है, उसी को संन्यास कहते हैं। संन्यास ग्रहण करने के विषय में मनु ने व्यवस्था दी है-
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान्परिव्रजेत् ॥
-मनुस्मृति 6/33
अर्थात् आयु के चौथे भाग में सभी प्रकार के संग-साथ को त्याग कर संन्यास ग्रहण करें।
यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 25 से 50 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ जीवन का भोग करने के कारण इंद्रियों को एक साथ वासनामुक्त करना बहुत कठिन है। इसलिए ऋषियों ने 50 से 75 वर्ष तक आयु के तीसरे भाग को वानप्रस्थ-आश्रम के रूप में वन में बिताने की व्यवस्था दी है। इस आश्रम में पत्नी को साथ रखा जा सकता है और इंद्रियों का संयम करते हुए सभी प्रकार के यज्ञ, हवन आदि कार्य किए जाते हैं तथा शेष रह गए ऋणों से मुक्त होने के प्रयास भी जारी रहते हैं। इसके बाद ही संन्यास की व्यवस्था है-
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत् । अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः ॥ अधीत्य विधिवद्वेदान्पुत्रांश्चोत्पाद्य इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत् ॥
धर्मतः ।
- मनुस्मृति 6/35-36
अर्थात् तीनों ऋणों-देवऋण, after और पितृऋण से मुक्त होकर मन को मोक्ष में लगाएं। ऋण चुकाए बिना जो मोक्षार्थी होता है, वह नरकगामी होता है। विधिपूर्वक वेदों को पढ़कर धर्म से पुत्रों को उत्पन्न कर और यथाशक्ति यज्ञों का अनुष्ठान करके तब चतुर्थ आश्रम में मन को लगाएं। उपर्युक्त विधान इसलिए है कि चतुर्थ आश्रम में संन्यासी के लिए कोई कर्म शेष नहीं रह जाता, उसका उद्देश्य तो कर्म से छूटना होता है-
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः । आत्मनैव सहाय्येन सुखार्थी विचरेदिह ॥
अर्थात् संन्यासी सदा आत्मा के ही चिंतन में लगा रहे; विषयों की इच्छा से रहित निरामिष होकर
एक देह मात्र की सहायता से सुख का अभिलाषी होकर संसार में विचरे । नारद परिव्राजकोपनिषद् में कहा गया है कि जिसमें शांति, शम, शौच, सत्य, संतोष, दयालुता, नम्रता, निरहंकारिता, इमहीनता भरी हो, वही संन्यास का अधिकारी है।
संन्यासी के लिए दी गई इन व्यवस्थाओं के बारे में भगवान् श्रीकृष्ण ने भी श्रीमद्भगवद्गीता के निष्काम कर्मयोग और सांख्ययोग अध्यायों में विस्तार से प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि जो कर्म के फल को न चाहकर करने योग्य कर्म करता है, वही संन्यासी और योगी है।
संन्यास की व्यवस्था हमारे ऋषियों द्वारा मोक्षप्राप्ति के लिए की गई अत्यंत वैज्ञानिक व्यवस्था है। कमली प्रकार समझने के लिए धर्म के मूल को समझना बहुत आवश्यक है। आत्मा की अमरता और जन्म में विश्वास हिंदूधर्म के दो आधारभूत सिद्धांत हैं।
अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों जन्म होता है। मनुष्ययोनि इनमें सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, किन्तु जीवनभर सुख-दुःख तो इस योनि में भी भोगने ही पड़ते हैं। इन सुख-दुःखों से भी आगे नौ महीने के गर्भवास की घोर यातना और बुरे कर्म बन पड़ने पर मृत्यु के बाद प्रेतयोनि का घोर कष्ट जीव को सहना होता है।
इन सभी कष्टों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि जीवन में पापकर्म न किए जाएं। यदि कोई पापकर्म हो भी गया है, तो उसका प्रायश्चित कर लिया जाए और जीवन को कर्मफल रहित कर लिया जाए। जब कर्म ही शेष नहीं होंगे, तो पुनर्जन्म भी नहीं होगा और आत्मा अपने मूल स्रोत परमात्मा के साथ मिलकर सदा-सर्वदा के लिए शांति और आनंद में समा जाएगी।
इन फलरहित कर्मों की साधना का नाम ही संन्यास है और आत्मा की मुक्ति ही संन्यास का परिणाम । व्यक्ति का जन्म कर्मफल के बंधन के कारण होता है, किंतु आत्मा के निवास के लिए शरीर की रचना तो माता-पिता के द्वारा ही की जाती है।
अतः मनुष्य पर सबसे पहला ऋण माता-पिता का होता है। इसे पितृऋण कहते हैं। माता-पिता शरीर के निमित्त होते हैं, लेकिन शरीर की रचना जिन तत्त्वों से मिलकर हुई है तथा जिन तत्त्वों को खा-पीकर यह बढ़ता उन तत्त्वों की रचना माता-पिता ने नहीं की है। वे तत्त्व देवताओं द्वारा दिए गए हैं। अतः उनका कर्ज चुकाना भी जरूरी है। इस ऋण को देवऋण कहते हैं।
- मनुस्मृति 6/49
माता-पिता के जिस रज और शुक्र के अंश से शरीर की रचना हुई है, वह रज-शुक्र उन्हें अपने माता-पिता की परंपरा से प्राप्त हुआ है। उस परंपरा को देने वाले समय के साथ-साथ मृत्यु को प्राप्त होते गए हैं,
किंतु उनके द्वारा दी गई सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान का अंश ऋण के रूप में हमारे पास है। इसे ऋषिऋण कहते हैं। इन तीन प्रकार के कर्मों से मुक्त हुए बिना हम किसी भी प्रकार की मुक्ति की कामना नहीं कर
सकते, इसीलिए संन्यास के लिए आयु के चौथे भाग की व्यवस्था की गई है। धार्मिक आचरण करते हुए गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति जीवन के सभी भोगों को पर्याप्त मात्रा में भोग लेता है।
उसके बाद वानप्रस्थ में इंद्रियसंयम रखते हुए 25 वर्ष का संन्यास आश्रम आरंभ होता है। जिसमें मन को नियंत्रित करके व्यक्ति कर्मफल से बचने की साधना करता है और मोक्ष प्राप्त करने को प्रयत्नशील रहता है।

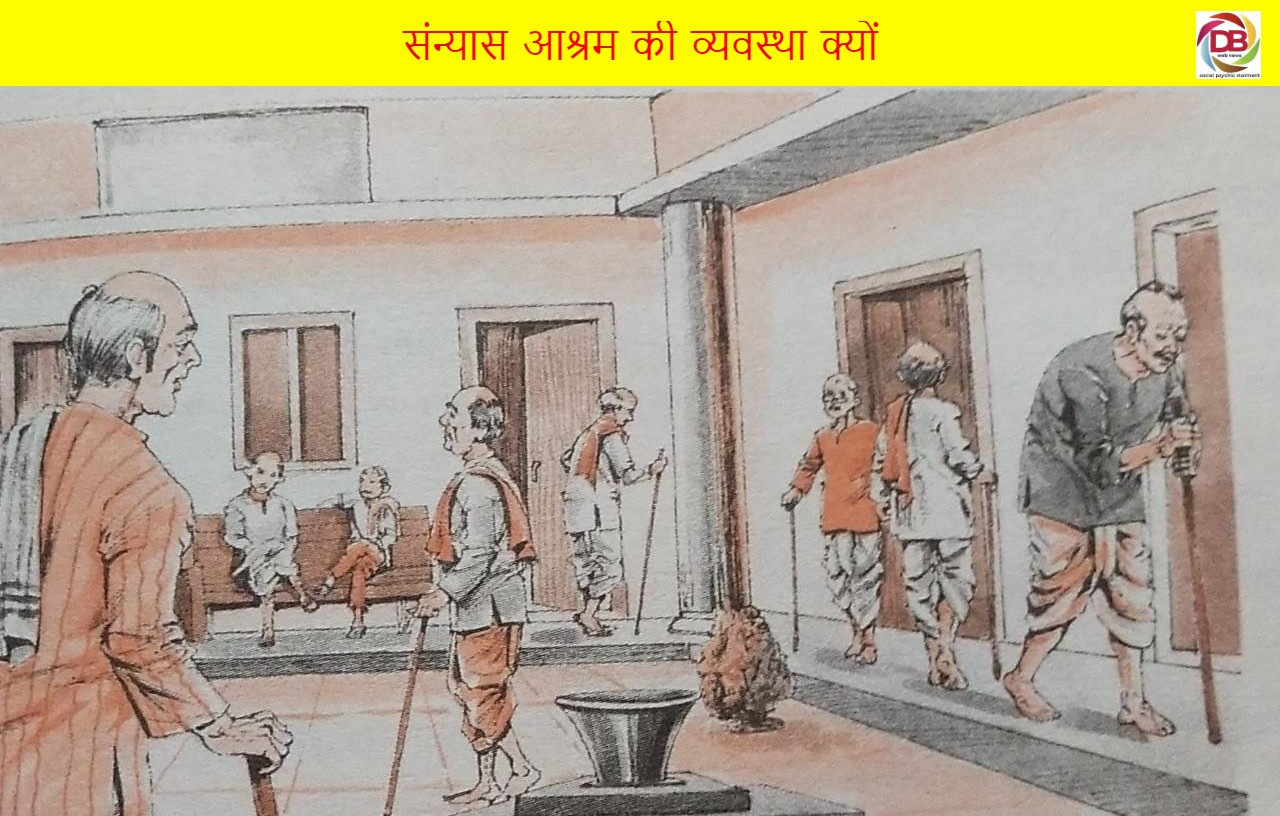







![श्री पूर्णेश्वर शिव सेवा फाउन्डेशन Shri Purneshwar Shiv Sewa Faundation [rag.no 623] को सहयोग करें](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfdvyQTN1LiLfyk2EGWqFH0Rw1ABfFO1sTmr91vJ5lYAK8YYnpR-nmQ-DcLBiEqUvm-Pte2eMfgTcFanZ_PBeoWesu8DafNhY-1fO9FfYWi78Jr2LhqzvD3bALHPu_FrJgAq40dK1Fw6drEibAJOSfeymapRPIbnNQCtMTGO9lKiNejzWwg7BCGN9oJdE/w150/IMG-20240108-WA0001.jpg)

कोई टिप्पणी नहीं